- +919468439002
- gups7dpn@gmail.com
- GUPS 7 DPN Block Bhadra
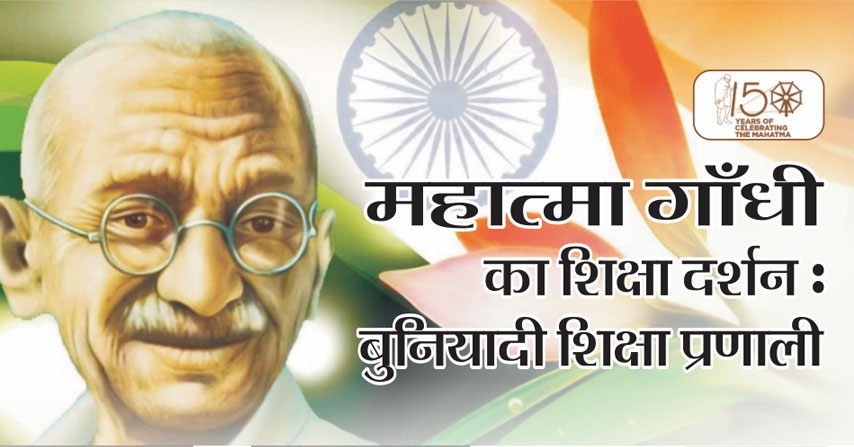
गांधी जी का शिक्षा दर्शन
गाँधी जी न केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे अपितु जीवन और समाज के अनेक क्षेत्रों में उनकी देन अमूल्य है। उन्होंने राजनीतिक क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक क्रान्ति को भी जन्म दिया और इसमें शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया। वे एक श्रेष्ठ विचारक थे। ‘बुनियादी शिक्षा प्रणाली’ उनके शैक्षिक विचारों का एक व्यावहारिक रूप है।
शिक्षा दर्शन के सिद्धांत
- सम्पूर्ण देश में 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए।
- शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिये ।
- शिक्षा विद्यार्थियों में समस्त मानवीय गुणों का विकास करे।
- शिक्षा द्वारा बालकों को बेरोजगारी से एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए।
- शिक्षा को बालक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिये।
- शिक्षा को बालक के शरीर, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना चाहिये।
- शिक्षा किसी लाभप्रद हस्तशिल्प से प्रारम्भ होनी चाहिये जो बालक को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बना सके।
- शिक्षण जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।
शिक्षा का अर्थ (Meaning of Education)
गाँधीजी का विचार था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित बने। वे मात्र साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। वे इसे ज्ञान या ज्ञान का माध्यम भी स्वीकार नहीं करते थे। गाँधी जी शिक्षा में न तो साक्षरता को स्वीकार करते थे और न ही ज्ञान को। उनके शब्दों में, “शिक्षा से मेरा अभिप्राय है- बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाये जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चतुर्मुखी विकास।”
शिक्षा के उद्देश्य (Aim of Education)
गाँधीजी ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया है-
(अ) तात्कालिक उद्देश्य । (ब) अन्तिम उद्देश्य ।
(अ) तात्कालिक उद्देश्य- ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं-
- (i) बालक की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करके उसके व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास करना चाहिये।
- (ii) बालक के चरित्र का निर्माण करना चाहिये।
- (iii) बालक को अपनी संस्कृति को व्यक्त करने का प्रशिक्षण देना।
- (iv) बालक को उच्च जीवन की ओर अग्रसारित करना चाहिये।
- (v) उसे जीविकोपार्जन के योग्य बनाना।
(ब) अन्तिम उद्देश्य– गाँधीजी के अनुसार, शिक्षा का अन्तिम उद्देश्य है। “अन्तिम वास्तविकता का अनुभव, ईश्वर और आत्मानुभूति का ज्ञान। “
शिक्षण विधि (Method of Teaching)
गाँधी जी की शिक्षण-विधि निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित है- (i) करके सीखना। (ii) अनुभव द्वारा सीखना। (iii) सीखने की प्रक्रिया में समन्वय ।
गाँधीजी चाहते थे कि बालकों को वास्तविक परिस्थितियों में सिखाया जाये। इसके लिये वे किसी हस्त-कौशल अथवा उद्योग कार्य, प्राकृतिक पर्यावरण या सामाजिक पर्यावरण को शिक्षा का केन्द्र बनाने तथा समस्त ज्ञान व क्रियाओं को उनके माध्यम से विकसित करने पर विशेष बल देते थे।
शिक्षक का स्थान (Place of Teacher)
गाँधीजी के अनुसार, एक शिक्षक, आदर्श शिक्षक तभी बन सकता है जब वह शिक्षण कार्य को व्यवसाय के रूप में नहीं, वरन् सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करे। उसे सत्य आचरण करने वाला, सहिष्णु, ज्ञान का भण्डार एवं धैर्यवान होना चाहिए।
शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन (Estimate of Educational Philosophy)
गाँधीजी के शिक्षा दर्शन का आधार आदर्शवाद है तथा प्रकृतिवाद एवं प्रयोजनवाद मात्र उसके सहायक के रूप में हैं। गाँधीजी का शिक्षा दर्शन बालक की प्रकृति को विशेष महत्त्व देता है। इसलिये वह प्रकृतिवादी है और क्योंकि यह दर्शन बालक को उसकी रुचि के अनुसार सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्रिया करके सीखने पर बल देता है। अतः वह इस अर्थ में प्रयोजनवादी है। आदर्शवाद इस अर्थ में है क्योंकि गाँधीजी शिक्षा के अन्तिम उद्देश्य को आत्मानुभूति मानते हैं, वे बालकों का सत्य और अहिंसा का विचार पढ़ाना चाहते हैं।
गाँधी जी का शिक्षा दर्शन का पता उनके शैक्षिक विचारों से लगाया जा सकता है। गाँधी जी का शिक्षा दर्शन आदर्शवादी प्रयोजनवाद तथा प्रकृतिवाद तीनों से ही प्रभावित है। गाँधी जी के अनुसार, शिक्षा के अर्थ पर यदि ध्यान दिया जाए तो गाँधी जी के अनुसार, “शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इस परिभाषा में गाँधी जी ने शरीर जोकि प्रकृतिवाद का तत्त्व है, मन जोकि प्रयोजनवाद का तत्त्व है तथा आत्मा जोकि आदर्शवाद का तत्त्व है। इस प्रकार गाँधी जी की शिक्षा के विचारधारा में प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद तीनों का ही समन्वय पाया जाता है। इसी प्रकार गाँधी जी के द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्यों में प्रमुख है- चारित्रिक विकास, जोकि प्रकृतिवाद का द्योतक है। व्यावसायिक विकास प्रयोजनवाद से प्रभावित है तथा आध्यात्मिक विकास आदर्शवाद का मूल तत्त्व है। गाँधी जी का शिक्षा दर्शन ही नहीं अपितु जीवन दर्शन की प्रकृतिवाद प्रयोजनवाद तथा आदर्शवाद का समन्वय है। गाँधी जी ने सत्य अहिंसा तथा प्रेम का विचार या दृष्टिकोण को स्वीकार किया है तथा सन्देश भी दिया है जिसमें सत्य आदर्शवादी विचार है। अहिंसा प्रकृतिवादी विचार है तथा प्रेम प्रयोजनवादी विचार है। इस प्रकार गाँधी जी का सम्पूर्ण दर्शन आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोजनवाद का समन्वय है।

